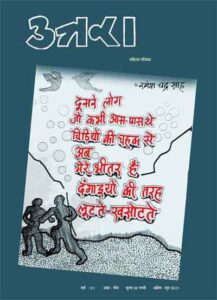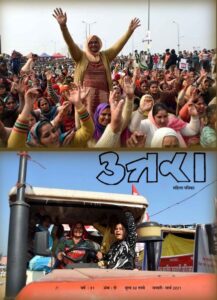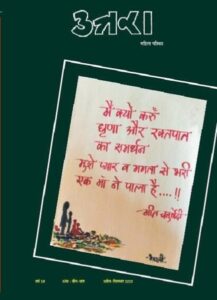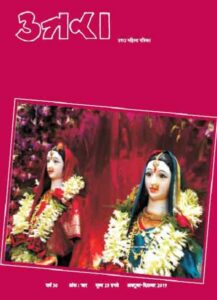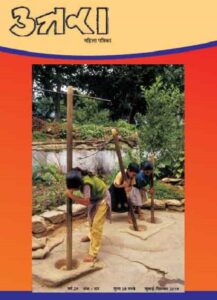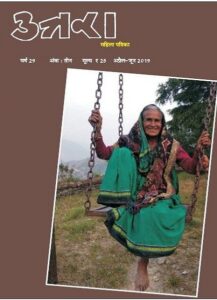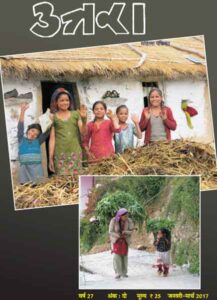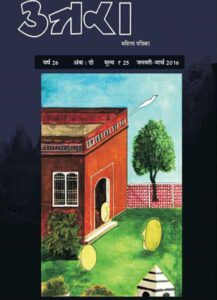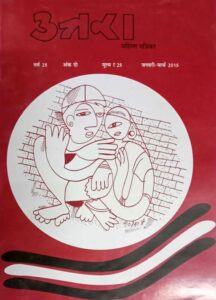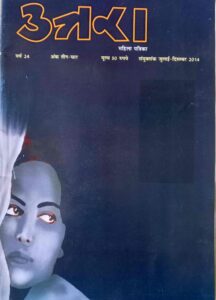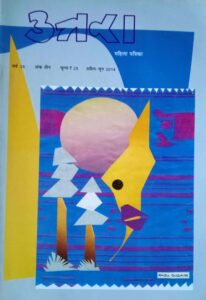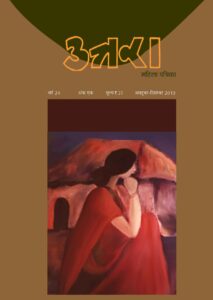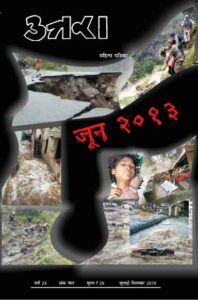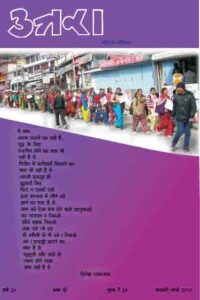पंचधार के फटने का इंतजार
शीला रजवार
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विद्यासागर नौटियाल का 20 सितम्बर 1933 को टिहरी के माली देवल गाँव में जन्म हुआ। उनका बचपन अपने पिता के साथ टिहरी रियासत के घनघोर जंगलों के बीच बीता और घर में ही प्रारम्भिक शिक्षा हुई। 11-12 वर्ष की उम्र में वे पढ़ने के लिये टिहरी शहर आ गये। 13 वर्ष की उम्र में वे गढ़वाल में राजशाही और सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन में शामिल हो गये ओर जेल भी गये। अपने इसी जुझारू व्यक्तित्व के कारण आजाद भारत में भी बहुत बार जेल गये। आपने उच्च शिक्षा देहरादून और बनारस में ली। 1980 में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गये।
1954 में इनकी पहली कहानी भैंस का कट्या, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उलझे रिश्ते, सूरज सबका है, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बायां है और यमुना के बागी बेटे। इनकी औपन्यासिक कृतियाँ हैं। देशभक्तों की कैद में संस्मरण तथा मोहन गाता जाएगा आत्मकथा अंश है। भीम अकेला उस समय की संस्मरणात्मक यात्रा का वृत्तान्त है जब इन्होंने विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र का भ्रमण किया था। सम्भवत: वह पहले विधायक होंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र की पैदल यात्रा की। आपकी कहानियों- परीदेश की कहानियाँ, भैंस का कट्या, पीपल के पत्ते और घास का नाट्य रूपांतर और मंचन हो चुका है। फट जा पंचधार कहानी अनेक मंचों पर प्रस्तुत की जा चुकी है। एक कहानी सीरियल के अंतर्गत सोना कहानी पर लघु फिल्म बनी जिसका दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर कई बार प्रसारण हो चुका है।
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल की कहानियों को पढ़ते हुए इस बात का गहराई से अहसास होता है कि इनके नारी पात्र सीधे-सीधे जीवन के संघर्षों और पीड़ाओं में जी रहे हैं। यद्यपि नौटियाल जी लेखन के साथ-साथ राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। इस तरह उन्होंने एक वृहत्तर समाज में भागीदारी की। वामंपथी विचारधारा वाले नौटियाल जी विधायक बनने के बाद भी अपने अंचल के जन-जीवन की संवेदनाओं से जुड़े रहे हैं। अपने क्षेत्र लोगों के जीवन के दु:ख दर्द उन्हें हमेशा सालते रहे। स्मृति बिम्बों में हमेशा जीवित, टीसते और रिसते।
हमारी सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली, सामाजिक रीति-रिवाज, मान्यताएं और भौगोलिक-र्आिथक परिस्थितियाँ किस तरह से और कितने प्रकारों से स्त्री जीवन को प्रभावित करती हैं इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रण अन्तर्मन की गहराइयों के साथ नौटियाल जी अपनी कहानियों में करते हैं।
कहानियों की चर्चा करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि वह टिहरी जो लेखक के रचनाकर्म में हर जगह मौजूद रही है, सामंती परिवेश और वंशानुगत शासन की पारम्परिक विरासत को थामे हुए थी। ऐसे समाज में स्त्री शोषण का यह रूप इन कहानियों में बहुत स्पष्ट है। लेकिन यह भी सच है कि शोषण जितना ज्यादा होगा विद्रोह की सम्भावनाएँ और अवसर भी उतने ही होंगे। इस विद्रोह की अनुगूँज भी इन कहानियों में सुनाई पड़ती है।

फट जा पंचधार की भूमिका में वे स्वयं लिखते हैं- ‘मेरी रचनाओं का (उपन्यासों सहित) मूल्यांकन करने के लिए इस बात पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है कि मेरा जन्म एक रियासत के अन्दर, पारम्परिक तौर पर एक परिवार की दासता में जकड़े सामन्ती समाज में हुआ था। मेरे लोग ‘जनता’ नहीं, ‘प्रजा’ थे। राजाओं के सामने मेरे लोगों को प्रार्थी लिखने का हक नहीं था, अपने को ‘गुलाम’ की संज्ञा से विभूषित करना होता था, स्त्री की यह नियति किसी भी देशकाल के समाजों में परिव्याप्त है जहाँ उसे अपने बारे में सोचने या निर्णय लेने का हक/अवसर नहीं मिला।
नौटियाल जी की कहानियों में छपी टिहरी रियासत की पृष्ठभूमि में स्त्री के विविध रूपों, कार्य का प्रकार, काम का बोझ, सास-बहू का सम्बन्ध, जीवन शैली, रीति-रिवाज, बेटी को बेचने का चलन (मूल्य लेने की प्रथा) पति का रवैया, दहेज और उससे जुड़ी मानसिकता, सवर्ण गरीब महिला की स्थिति और सामाजिक दबाव, सम्पन्न परिवार की होने का अर्थ, अर्थ लोक किवदंतियों-कथाओं में उजागर होती उनका आधार बनाती स्त्री की स्थितियाँ, आपसी सम्बन्धों का चित्रण है।
महाराजा काफू शाह का आत्मघात इसी सामन्ती समाज की नजर में स्त्री क्या है, इस बात का कच्चा चिट्ठा है। काफूशाह को वैरागी होने से बचाने के लिये दरबार में राज्य की प्रजा की अविवाहित कन्याओं की परेड और सुन्दरियों का चयन। परेड का एक सौ सात दिन तक चलना और इस आदेश को राजाज्ञा न मानकर भगवान बद्रीनाथ की आज्ञा मानने का संदेश राजा की निरंकुशता का परिचायक है। दूसरी ओर रूपदेई के प्रति काफूशाह का आकर्षण और मिलने पर काफूशाह के पिता की उसके प्रति जन्मी आशक्ति पिता-पुत्र में भेद पैदा कर देती है। इसी क्रम में पिता-पुत्र दोनों का रूपदेई के प्रति आसक्त होना और उसके लिये युद्ध की स्थिति रूपदेई के लिये राजा का राज्य त्यागना और रूपदेई की राजा के साथ ही विवाह करने की प्रतिज्ञा के आड़े आने पर अन्त: पुर में बंदी बना लेना। यह सामन्ती समाज का एक चेहरा है। एक और कहानी ‘पीपल के पत्ते’ में प्रशासनिक तंत्र में एक गरीब की मजबूरी व्यक्त हुई है। इसमें मेहनतकश किसान और नौकरीपेशा शहरी लोगों की आरामतलब जिन्दगी की विसंगति है। उस पर भी पति रामू पत्नी रामी को ‘जनानी जात अंधियारी रात’ मानकर चलता है। रामू उन शहरी सुविधा सम्पन्न लोगों के प्रति ईष्र्या भाव व्यक्त करता है। ”दिन भर दफ्तर में बैठे रहे, काम नहीं काज नहीं, न घास की फिकर न लकड़ी की। खेती न बाड़ी, मौज मस्ती की जिन्दगी।” रामी का ”और हम मेहनत न करें तो ये भूखों मर जाएँ।” कथन श्रम की महत्ता को व्यक्त करता है। यह श्रम नौटियाल जी की अन्य कहानियों में बड़े दारुण रूप में मौजूद है। ‘समय की चोरी’ कहानी में डबली घर-जंगल, खेत-खलिहान जानवर सभी के कामों में जिस तरह डूबी है- वह इस अंचल की अन्य सभी स्त्रियों की कहानी भी है। जहाँ अच्छा भोजन या अच्छी नींद एक सपना मात्र है और इन सबके बारे में उसे सोचने की भी इजाजत नहीं है। दही बिलोने का काम उसका है पर मक्खन लग जाने पर सास डबली को छुट्टी दे देती है। उसे हुक्म होता है कि सोने चली जाए। डबली को नहीं मालूम वह मक्खन कौन खाता है। मक्खन बाजार में बेचा जाता है या घर का कोई सदस्य खाता है। डबली ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की।’ उसे अपने बारे में सोचने की न फुर्सत है न जरूरत- फर्श पर लगातार खड़े रहने वाले पशु के खुरों में औरतों के पांवों की तरह रोग लग सकता है। कादई लग सकती है।…. दुधारू भैंस का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। उसके खुरों पर रोग लगने पर मुसीबत हो जाती है। औरत के पाँवों की कादई कोई बात नहीं।’ वह डबली जब ढेर सारे पत्ते तेजी से काट लेती है तब उसके पास समय बच जाता है। वह घर नहीं जाती, वह आराम करना चाहती है। आराम जो उसे जिन्दगी में कभी मयस्सर नहीं हो पाता। लेकिन वह फिर यह सोचकर कि उसे दोपहर के भोजन के बाद घास लेने भेजा जायेगा इसलिए घास लेने आने के वक्त वह आराम कर लेगी, घास काटने में जुट जाती है। ढेर सारी घास काटकर वह रख देती है, यह दुआ मनाती हुई कि कोई उसकी घास चोरी न करे। इस बचे समय में बहुओं से खूब बातें करने, जरूरत पड़ने पर किसी बहू को घास देने की सुखद कल्पना करती हुई घर लौटती डबली मान रही है कि उसरे समय चुरा लिया है अपने लिये और मना रही है उसकी घास चोरी न हो।
story fatja panchdhar
ऐसे ही ‘मूक बलिदान’, ‘अपनी पारी मौन’, ‘सोना’, ‘उस चिड़िया के बोल’ की स्त्रियाँ अपने जीवन में संघर्ष में बिना किसी शिकायत के नजर आती हैं। वे न केवल शिकायत नहीं करती वरन् अपने लिये निकाला समय उन्हें अपराध बोध से ग्रस्त कर जाता है। ‘बहुओं का ईमान’ की परोती जब थकान के दबाव में धान काटते-काटते सो गयी तब पड़ोस की बुढ़िया द्वारा जगाने का या वह- ‘उसके पाँव पकड़कर बोलती है’, ‘जी! हाथ जोड़ती र्हू, पाँव पड़ती हूँ। मेरी सास से मत कहना’ ‘नहीं कहूंगी’ का वादा करने के बावजूद वह सास से शिकायत कर देती है। ‘बहुओं का कोई ईमान नहीं होता। अभी तक सो रही थी वह आड़ी के नीचे’ सास ने उस दिन परोती को करछी भी मार दी। उसके हिस्से का खाना भैंस को खिला दिया। यही परोती जब सास बनीं एक दिन बहू की शिकायत बेटे से करती है कि उसके बक्से में चोरी से रखी गई मिठाई की पोटली मिली और कहती है ”बहुओं के ईमान का कोई भरोसा नहीं होता। सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की स्थिति को उजागर कर देता है जो सदियों से इसी तरह चली आ रही है।) ‘समय की चोरी’ में भैंस के खुर में कादई नहीं लगनी चाहिए, चाहे स्त्री के लग जाये और ‘बहुओं का ईमान’ में सजा के रूप में बहू के हिस्से का खाना भैंस को खिला देना उनकी पशुओं से भी गयी बीती हालत को दर्शाता है।
अपनी पारी मौन में सबला का पिता गाय बेचने से तो इंकार कर देता है लेकिन अपने समवयस्क बूढ़े से सौदा करते हुये सबला को दस हजारिया बाँह कहते हुए मोलभाव करता है।
story fatja panchdhar
नौटियाल जी की कहानियों की स्त्री के हिस्से में बंधुआ मजदूर सा श्रम तो है ही, साथ ही सामाजिक रीतियाँ और बंधन भी हैं जो उसके कष्टों में और भी बढ़ोत्तरी कर देते हैं। ‘छूट’ कहानी स्त्री की इसी छटपटाहट की कहानी है। पति के मरने के बाद सौरा जेठ के परिवार में हाड़ तोड़ परिश्रम करती रही। वह छूट पाना चाहती है। अपने भाई से भी कहती है लेकिन वह विवाह में लिया धन लौटाने की स्थिति में नहीं थे। पर सोचा कि उसे नये घर में बेचकर मिले पैसे को कौरा के जेठ को दे देंगे जिससे उसे छूट मिल जायेगी। कौरा तो जेठ के ही घर में थी। वह उसे बेटी की तरह विदा करने की बात कहकर अदालत से छूट दे देने को कहता है लेकिन वह उसके लिये लुगथ्या को पति बनाकर ले आया। कौंरा उसी घर में रहने के लिये विवश हो गई। पाँव की जूती कहानी की शारदा अफसर की पत्नी है लेकिन शहर से गाँव लौटने पर अपने जूते छिपाकर घर जाती हैं क्योंकि उसकी गाँव की महिलाओं ने जूते-चप्पल नहीं पहने हैं। यह यथास्थिति से छूटने की चाह होते हुए भी छूट न पाने की मानसिकता है। यह बामणपन टूटे की भवानी परिस्थितियों के साथ-साथ संस्कारों से भी दबी हुई है। वह बार-बार चाहती है कि अन्य महिलाओं की तरह खुला व्यवहार कर सकें लेकिन ब्राह्मण होना उसे रोक देता है। वह सर धोने के लिए भीमल की दो टहनियाँ तोड़ लेना चाहती है। वह यह भी सोचती है कि अपने पति से कहेंगी कि ‘कहीं से दो शाखें भीमल की ले आ’। निरन्तर दोनों बातें उसके अन्दर चलती रहती हैं। लेकिन न वह खुद भीमल की शाखें ला पाती है, न अपने पति से कह पाती है। कहानी का अंत आजादी की सोच का रूप बन जाता है। वह सोचती है अपने बाल ही काट ले या अंजाम की परवाह किये बिना किसी के पेड़ से भीतर की दो डाल काट ले। होती हो गलियों की बौछार तो हो यह तो शगुन ही होगा। गाँव में फैली हुई, खुली सार के अन्दर एक नयी जिन्दगी की शुरुआत। इस सोच का मुखर रूप हमें फट जा पंचधार कहानी में मिलता है। ‘पंचधार’ वह स्थान है जिस पर बैठकर पंच निर्णय लिया करते थे। यूँ तो पंचों में परमेश्वर का वास होता है किन्तु इन पंचों का फैसला कितना न्यायसंगत होता है? इस पर कहानी सवाल उठाती है- इकतरफा फैसला सुनाने वाली उस पंचायत में मैं, मेरे जन्मदाता, मेरे जने कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे…. वे फैसला सुनाते, हम सुनते। सुनते और बेबस होकर अमल करते। कहानी बहुपति विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालती है। जिसमें एक स्त्री के अनेक पतियों में पति उससे बहुत छोटे होते थे। वे अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये विवाहेतर सम्बन्ध बना लेते। कहानी की नायिका के एक युवा ससुर की दूसरी औरत से सम्बन्ध बनाने के जुर्म में हत्या कर दी जाती है। हत्यारा पंचायत को सही बात बता देता है। पंचायत ने उसे कोई सजा नहीं दी, बरी कर दिया। उसकी उम्र सत्तर वर्ष थी। उसका युवा भाई मर गया था। उसकी पत्नी जवान थी वह अपने बूढ़े पति से छूट चाहती थी। लेकिन, पति के जीवित रहते पंचायत छूट होने के लिये तैयार नहीं थी। दिलदेई के पिता और उसके भी पिता सभी मालिकों के कर्ज तले डूबे हुए। रात-दिन भूखे-प्यासे, नंगे-अधनंगे खटते। कभी उऋण नहीं हो पाते। पंडित कहते वे कर्जदार मरे हैं इसलिए नरक में कर्ज चुकाओ तो उन्हें मुक्ति मिले। पीढ़ियाँ कर्ज चुकाने के लिये पिसती और कर्जदार ही मर जातीं। बकौल ब्राह्मणों के नरकवासी हो जाती। दिलदेई की माँ अपने पति को नर्क से छुड़ाना चाहती थी। वह दिलदेई को ऊँची कीमत पर बेचकर (विवाह कर) अपने पति को छुड़ाना चाहती थी, ऐसे में वीरसिंह का प्रस्ताव स्वीकारते हुए बिना विवाह के वह वीरसिंह की हो गई। वीरसिंह ने सौदा किया कर्ज माफ कर दिया रक्खी के बदले। ‘माँ ने ‘जा’ और वीरसिंह ने ‘चल’ कहा और मैं वीरसिंह के पीछे हो ली। ….. मैं जा नहीं रही थी, ले जायी जा रही थी। मेरे कानों में ‘जा’ और ‘चल’ के स्वर जोर-जोर से गूँजने लगे थे। इतने जोर से और इतनी तेजी से कि मुझे लग रहा था कि ढोल-नगाड़े बज रहे हैं। ढोल से जा-जा-जा की और नगाड़़े से चल-चल-चल की आवाजें उठ रही हैं।’ रक्खी, वीरसिंह के साथ अलग घर में रहती है। 30 वर्ष तक वह उसके साथ रही। उसका घर-खेत-पशु धन सम्भालती सहेजती और बढ़ाती। नहीं बढ़ा सकी तो अपनी वंश-बेल- दो बार गर्भवती हुई लेकिन वीरसिंह ने ताकत की दवा के नाम पर उसे गर्भपात की दवा खिला दी। ‘धर्मा’ जो पहाड़ के कष्टों से छटपटाती स्त्रियों को बहला-फुसलाकर, भगाकर कोठों में बेच देता था, रक्खी को भाग चलने के लिये उकसाता रहा पर वह नहीं भागी। वह वीरसिंह की एकनिष्ठ होकर उसके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। ‘दिलदेई’ मर गई। वीरसिंह के बड़े भाई के अलावा अन्य भाई भी मर गये। बड़ा भाई हयात साठ वर्ष की उम्र में सोलह-सत्रह साल की रत्ती को ब्याह लाया। रत्ती सामाजिक रीति के अनुसार वीर्रंसह से अपना हक माँगने लगी। पंचायत लगी। रक्खी गुहार लगाती रही। वीर्रंसह ने अपनी अशुद्धि और रक्खी के लिये अपनी जिम्मेदारी की बात उठाई, लेकिन सवाल समाज और सामाजिक रीति-रिवाजों की रक्षा का था। वीर्रंसह की ‘चान्द्रायण’ शुद्धि कर उसे बिरादरी में शामिल कर दिया गया। रत्ती की शुद्धि नहीं हो सकती थी और न ही वह गाँव में रह सकती थी, खेत का एक टुकड़ा, एक झोपड़ी उसे नहीं मिल सकती। क्योंकि ऐसे तो खेत-खलिहान बँट जायेंगे। रक्खी के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। कहानी के अंत में रक्खी बस इतना ही चाहती है कि ‘पंचधार फट जाए’। भूकम्प का एक झटका आए, तगड़ा भूचाल और इस पहाड़ का जोड़-जोड़ हिल उठे।…. और पंचधार खण्ड-खण्ड हो जाय। …. मैं उसी भूचाल का इन्तजार कर रही हूँ। ”मैं उसी दिन को देखने के लिये जिन्दा हूँ।”
पंचधार के फटने की कामना या बामणपन के टूटने की कामना करती ये स्त्रियाँ अपने जीवन संघर्षों और सामाजिक प्रताड़नाओं को झेलने के बाद एक व्यापक बदलाव की कामना करती नजर आती हैं। एक स्त्री का दु:ख, उसकी पीड़ा, उसके जीवन की विसंगतियाँ एक सार्वभौग शोषण का रूप ले लेती हैं जिसका प्रतिकार व्यवस्था में समूल परिवर्तन और जर्जर तथा मानवीय अधिकारों का हनन करने वाली मानसिकता से ग्रस्त सामाजिक मूल्यों व रीति-रिवाजों को नष्ट कर ही किया जा सकता है।
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विद्यासागर नौटियाल का 20 सितम्बर 1933 को टिहरी के माली देवल गाँव में जन्म हुआ। उनका बचपन टिहरी रियासत के घनघोर जंगलों के बीच बीता और घर में ही प्रारम्भिक शिक्षा हुई, 11-12 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिये टिहरी शहर आ गये। 13 वर्ष की उम्र में वे गढ़वाल में राजशाही और सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन में शामिल हो गये ओर जेल भी गये। अपने इसी जुझारु व्यक्तित्व के कारण आजाद भारत में भी बहुत बार जेल गये। 1980 में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गये। आपने उच्च शिक्षा देहरादून और बनारस में ली।
1954 में इनकी पहली कहानी भैंस का कट्या, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बाया है और यमुना के बागी बेटे। इनकी औपन्यासिक कृतियाँ हैं। देशभक्तों की कैद में संस्मरण तथा मोहन गाता जाएगा आत्मकथा अंश है। आपकी कहानियों परीदेश की कहानियाँ, भैंस का कट्या, पीपल के पत्ते और घास का नाट्य रूपांतर और मंचन हो चुका है। फट जा पंचधार- कहानी अनेक मंचों पर प्रस्तुत की जा चुकी है। एक कहानी सीरियल के अंतर्गत सोना कहानी पर लघु फिल्म बनी जिसका दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर कई बार प्रसारण हो चुका है।
story fatja panchdhar
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें