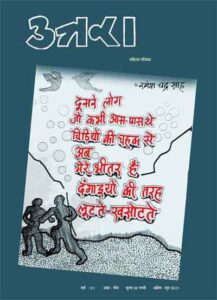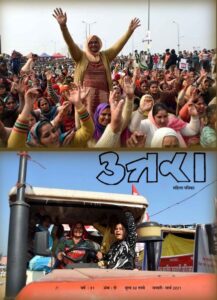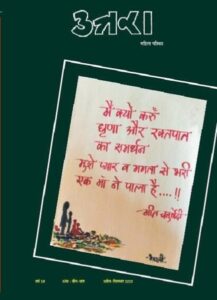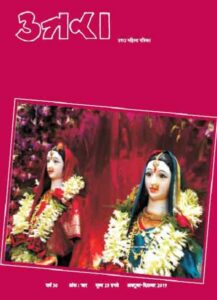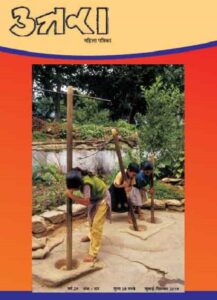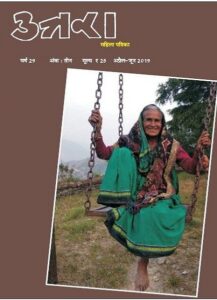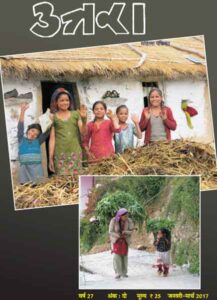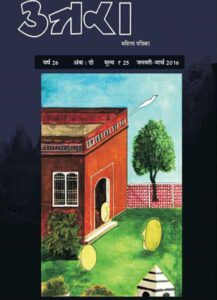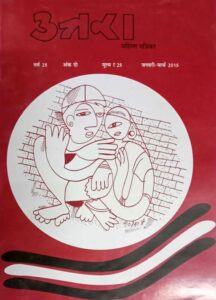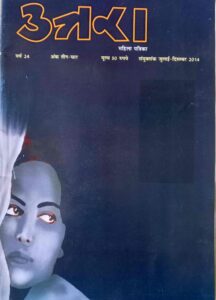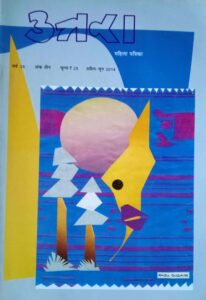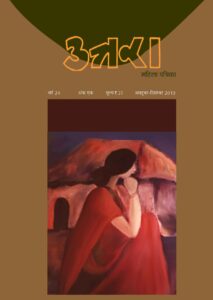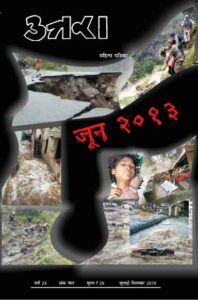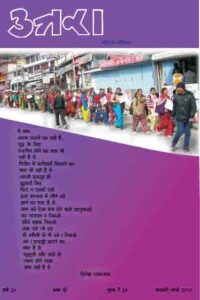दिशानिर्देशों से विधेयक तक
जया पांडे
संसद के मानसून सत्र (2012) के अंत में एक विधेयक ने कानून का रूप ले लिया। यह विधेयक है ‘कार्यस्थल पर यौन शोषण पर रोक’ (Prevention Prohibition Redressal) यह कानून वस्तुत: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (1997) जिन्हें ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ के नाम से ही जाना जाता है, का ही पुष्टीकरण है। हालांकि ये निर्देश उसी प्रकार काम कर रहे थे, जो एक कानून करता परन्तु कानून बनने के बाद इसकी प्रभावकारिता में अवश्य ही वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान है। निर्देशों के ही माध्यम से सरकारी तथा कारपोरेट सेक्टर में उचित कार्यवाही नहीं हो सकती थी। राष्ट्रीय महिला आयोग और सिविल सोसाइटी के प्रयासों से ही यह सम्भव हो पाया कि अब एक ऐसा कानून देश में है जो कार्यस्थल में महिलाओं को यौन शोषण के खिलाफ न्याय दे पायेगा। वे ऐसे माहौल में काम कर सकेंगी जिसमें कहीं से भी उन्हें धमकी का अहसास न हो।
यौन शोषण एक गम्भीर समस्या है। महिलाएँ रोजमर्रा की जिन्दगी में इसका शिकार होती हैं। दफ्तर हो या घर, सार्वजनिक स्थल हो या ट्रांसपोर्ट, गली, मुहल्ला, सड़क कहीं भी महिला को इसका शिकार होना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर इस प्रकार का शोषण महिलाओं को असुरक्षित बनाता है। इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। शिकायत होने पर कैरियर प्रभावित होता है। प्रमोशन पर प्रभाव पड़ता है, वेतनवृद्धि रोक दी जाती है। यह कहीं न कहीं एक व्यक्ति के निर्भय होकर काम करने पर सवाल पैदा करता है। नया कानून इसी मुद्दे से जुड़ा है। वस्तुत: जिसे हम बदलाव की बयार मान रहे हैं, वह इन महिलाओं के मन में है, जो अपने कैरियर के बारे में सोच रही हैं, ऊँचाइयों तक जा रही हैं तथा कुछ कर दिखाने की ललक जिनमें है। यह बदलाव स्त्रियों में ही आया है। पुरुष वर्ग इस नये बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते किसी न किसी रूप में हावी होने का पारम्परिक अधिकार ही अवांछनीय यौन व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए ही कानून की आवश्यकता है, जो नई आदतों का सृजन करें और ये आदतें ही स्वभाव बन जायें।
इस कानून का महत्व इसकी प्रस्तावना में है जो स्पष्ट शब्दों में घोषित करती है कि यौन शोषण महिलाओं के जीवन तथा समानता के अधिकार का हनन है। सुरक्षित तथा स्वस्थ माहौल में काम करना महिलाओं का अधिकार है जिसमें वे निर्भय होकर समाज को अपना योगदान दे सकें। ‘यौन शोषण’ की जो परिभाषा कानून में दी गई है वह भी सूक्ष्म है। यौन शोषण से तात्पर्य है: यौनिकता पर आधारित सोचा समझा आवांछनीय व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिसे आप पसन्द नहीं कर रही हैं और साथ ही जिसके पीछे दूसरे पक्ष ने सोची समझी रणनीति अपनाई हो। यह शारीरिक सम्पर्क, अश्लील फब्तियाँ, कामुक शब्द या इशारे कुछ भी हो सकता है। ‘शोषण’ के लिए अलग से परिभाषा उपलब्ध है, जो इस प्रकार है, वह यौनिक व्यवहार, जिसके न मानने पर आपके लिए धमकी हो या मानने पर आपको किसी लाभ से नवाजा जाना हो। ये सारी परिभाषाएँ एक ऐसी परिस्थिति का बयान करती हैं जो एक महिला को निर्भय होकर काम करने से रोकती हैं। किसी भी नागरिक को असहज, असुरक्षित तथा धमकी भरे माहौल में अगर काम करना पड़े तो यह मानव-मूल्यों की सामान्य जरूरतों को ही नहीं समझना है।
कानून में दो स्तरों पर प्रबन्धन की व्यवस्था की गई है। पहला हर कार्यालय में आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन तथा हर जिले में स्थानीय शिकायत समिति का गठन। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए नियोक्ता पर दबाव बनाया गया है कि हर कार्यालय द्वारा कुछ आचार संहिताएँ बनायी जांए जो अश्लील व्यवहार पर ‘जीरो टॉलरेन्स पर आधारित हो। जैसे अमेरिका की एक लाइब्रेरी में एक पोस्टर लगा था, जिसमें सिर्फ यौन अंगों को दिखाया गया था लेकिन वह किसी प्रकार का अश्लील संदेश नहीं दे रहा था। एक कर्मचारी की शिकायत भर से यह हटा दिया गया।’ यह कानून असंगठित क्षेत्र को भी लेता है क्योंकि कार्यस्थल का मतलब है, ऐसा व्यवसाय जो उत्पादन में लगा हो, समाज को कुछ सेवा प्रदान करता हो तथा कम से कम दस लोगों को नौकरी देता हो। कार्यालय के आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ में एक सदस्य स्वयंसेवी संस्थाओं से लिए जाने की बात कही गयी है। इन दोनों ही समितियों को सिविल कोर्ट की हैसियत दी गई है।
इस बिल की एक कमी है कि इसमें सेना तथा कृषि क्षेत्र को लिया जाना है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन क्षेत्रों में भी महिलाएँ असुरक्षित हैं। जहाँ भी महिलाओं के समानता तथा जीवन के अधिकार से खिलवाड़ हो, वह इसमें अवश्य ही आना चाहिए। बिल में अवांछनीय व्यवहार को ही अपराध माना गया है, वांछनीय को नहीं।
कल्पना शर्मा ‘हिन्दू’ में टिप्पणी देती हैं कि बिल पास हो गया परन्तु पास होने की प्रक्रिया में न संसद में बहस हुई और न ही मीडिया ने इसकी वांछित चर्चा की। बहस और चर्चा बिल के महत्व को अधिक व्यापक बनाती। महिलाएँ वैसे ही अपने से सम्बन्धित अधिकारों को नहीं जान पाती हैं। हर स्तर की महिलाओं तक सन्देश जाने के लिए जरूरी था कि इसमें व्यापक बहस होती।
यह जो समस्या है, यह कानून उस समस्या का एक प्रतिरोधात्मक उपाय है। इसकी जड़ें कहीं और भी हैं। सेक्स के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही हवस को जन्म देता है। जरूरत इस दिशा में भी सोचने की है। ‘सेक्स सम्बन्धों’ के प्रति स्वस्थ मानसिकता बनाने के लिए अन्य तरीके भी चाहिए। हर व्यक्ति का अपने शरीर पर अधिकार या स्वतंत्रता का अवश्य ही सम्मान होना चाहिए।
From Guidelines to Bill
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें