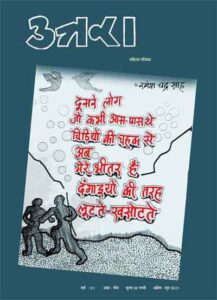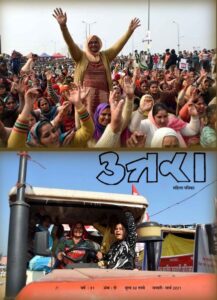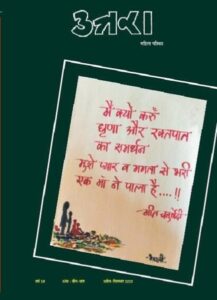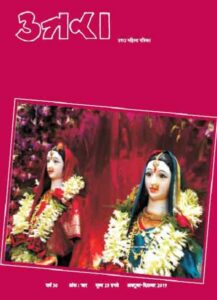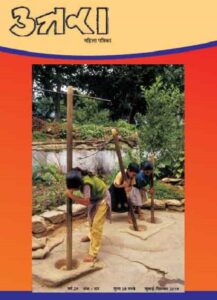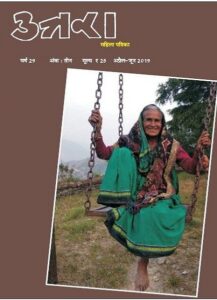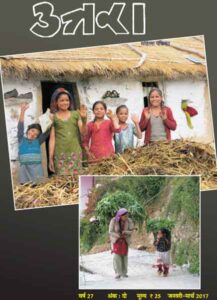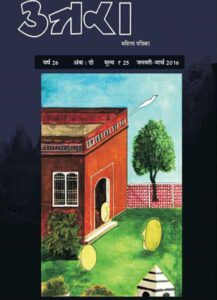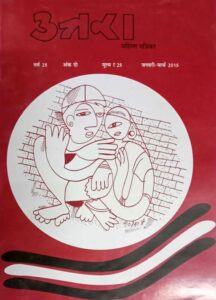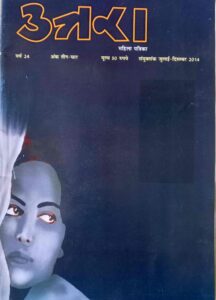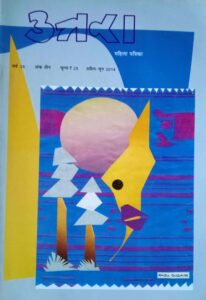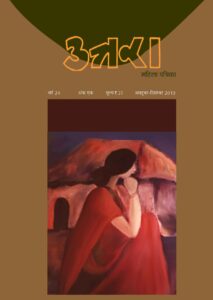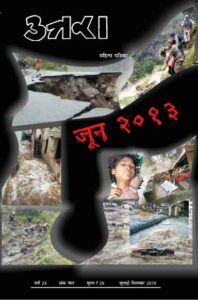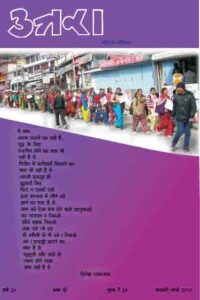इरावती की तरह उद्दाम थी इरावती कर्वे
जय निंबकर

इरावती नाम थोड़ा अटपटा है। मगर इस इरावती की तो पूरी जिन्दगी ही असामान्य रही। हरि गणेश कर्माकर की इस बेटी का जन्म 1905 में बर्मा में हुआ था। तब कर्माकर वहाँ बतौर इंजीनियर काम करते थे। यहाँ की इरावती नदी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए यह नाम चुना।
सात वर्ष की आयु में इरावती को पढ़ने के लिए भारत भेजा गया। इस तरह वह पुणे के एक आवासीय बालिका विद्यालय- हजूर पागा में पहुँच गईं। यह स्कूल महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए खोले गए प्रारंभिक विद्यालयों में एक था। इरावती को यहाँ एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई। यह थी आर.पी. परांजपे की बेटी शकुंतला। शकुंतला की माँ इरावती को अपने घर ले गई, जहाँ रहते हुए उनका साबका जीवन की दिशा ही बदल देने वाले विचारों से पड़ा।
इस बौद्धिक व नास्तिक घर में इरावती को नाना प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने और लोगों से मिलने का मौका मिला। इनमें एक थे जज बालकराम। उन्होंने इरावती के भीतर मानवशास्त्र (नृविज्ञान) को जानने की ललक पैदा की। बाद में इरावती ने इसी विषय को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर बौद्धिक दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसी दौरान उनकी मुलाकात दिनकर कर्वे से हुई, जो कालान्तर में उनके जीवन साथी बने। दिनकर देश में महिला शिक्षा और विधवा विवाह के ख्यातिनाम प्रवक्ता महर्षि धोंडो केशव कर्वे के दूसरे पुत्र थे और पुणे के फर्गुसन कॉलेज में रसायन विज्ञान पढ़ाते थे।
फर्गुसन कॉलेज से बीए करने के बाद इरावती ने समाजशास्त्र में एम.ए. किया। स्नातकोत्तर कक्षाओं में उनके निर्देशक बॉम्बे युनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक डॉ. जी.एस. घुर्ये थे। इरावती के पति अपनी पत्नी की बौद्धिक संभावनाओं से परिचित थे। इसलिए उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया। इस तरह इरावती बर्लिन पहुंच गईं, जहाँ उन्होंने 1930 में कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर एन्थ्रोपोलॉजी, यूजेनिक्स एंड ह्यूमन हेरेडिटी के निदेशक प्रो. यूजीन किशर के निर्देशन में मानवशास्त्र में पीएच.डी. की डिग्री हासिल की।
भारत लौटने के बाद उन्होंने बहुत थोड़े समय के लिए पुणे के एस.एन.डी.टी. कॉलेज में रजिस्ट्रार का पद संभाला। मगर उनकी रुचि प्रशासन में नहीं बल्कि शोध और अकादमिक कार्यों में थी। इसलिए जल्द ही वह त्यागपत्र देकर डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट चली आईं और यहीं उनकी आगे की पूरी पेशेवर जिन्दगी बीती।
उनके शोधकार्य के मुख्य विषय थे- ‘भारतीय क्या हैं? हम जैसे हैं, वैसे क्यों हैं?’ उन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए, वे पूरी तरह मानवशास्त्र के सामान्य उद्देश्य व लक्ष्य थे। जिन खास सवालों के जवाब उन्होंने तलाशने की कोशिश की, वे थे- 1. ऐतिहासिक, प्राक् ऐतिहासिक लोक आव्रजन के लिहाज से क्या भारत में विस्तृत सांस्कृतिक व भौतिक रूपरेखा की स्थापना की जा सकती है?, 2. भारत में विभिन्न स्थानों पर चिन्हित ऐतिहासिक एवं प्राक् ऐतिहासिक स्थलों को बसाने वाले लोगों के भौतिक स्वरूप किस प्रकार के थे?, 3. जाति क्या है? इस तरह के सवालों का जवाब खोजने की उनकी विधि नृतात्विक-ऐतिहासिक थी, जो उन्हें संभवत: बर्लिन की शिक्षा से मिली। उन्होंने चार क्षेत्रों में एक साथ शोध करना शुरू किया- पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, इंडोलॉजिकल स्टडीज, महाकाव्य व वाचिक परम्परा तथा विभिन्न क्षेत्रों का व्यवस्थित भौतिक नृतात्विक अध्ययन। इसके अलावा वे विभिन्न भाषाई इलाकों का विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन भी कर रही थीं।
Iravati Karve was as boisterous as Iravati
इरावती कर्वे ने महसूस किया कि समूचे भारत के लोगों का आपाधापी में अध्ययन करने के बजाय किसी एक इलाके के लोगों के बारे में व्यवस्थित ढंग से जानना ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे वे किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र की जातीय बनावट के बारे में ठीक से जान पाएंगी। वह किसी आदिम समूह या जाति समूह के बारे में नहीं जानना चाहती थीं। उनका कहना था कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के सौ नमूनों से हम अंतर्विवाह करने वाली ब्राह्मणों की एक दर्जन उप जातियों के जीनपूल के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते।
दो प्रमुख ब्राह्मण उप जातियाँ- चितपावन तथा देशस्थ ऋग्वेदी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दूसरी वाली तो मराठों के काफी नजदीक है। इसलिए वे इस बात की बहुत मजबूती से वकालत करती थीं कि नृतात्विक अध्ययन के लिहाज से भारत में नमूने जाति के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि जाति समूहों के आधार पर। इस प्रकार जाति को अध्ययन की इकाई के रूप में लेने के कर्वे के विचार ने भारतीय नृविज्ञान में मानो क्रांति ला दी।
कर्वे ने ऋग्वेद, अथर्ववेद और महाभारत में वर्णित रिश्तेदारी के वर्णन और उपयोग का भी अध्ययन किया। उन्होंने गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से आंकड़े एकत्र किए। उनका यह अध्ययन एक पुस्तक के रूप में सामने आया, जिसका नाम है- किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया (1953)। तीन खंडों में फैला यह विशाल अध्ययन सांस्कृतिक नृविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है और इस विषय में शोध करने वालों के लिए जरूरी संदर्भ के रूप में प्रतिष्ठित है।
कर्वे के शोधकार्य ने उन्हें भारत और दुनियाभर में प्रतिष्ठा दिलवाई। 1957 में वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस के नृविज्ञान खंड की अध्यक्ष चुनी गईं। लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ने उन्हें मानद लेक्चररशिप प्रदान की।
नृविज्ञान में उनके प्रमुख योगदान कई पुस्तकों के रूप में सामने आए। इनमें प्रमुख हैं- हिन्दू सोसाइटी, एन इंटरप्रेटेशन, जिसमें उन्होंने भारत के जातीय ढांचे को समझने के सूत्र दिए। इसके अलावा ‘किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया’तथा ‘महाराष्ट्र, लैंड एंड पीपुल’भी उनकी चर्चित कृतियाँ हैं। उन्होंने महाभारत पर मराठी में ‘युगान्त’नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। इस पुस्तक में विभिन्न पौराणिक चरित्रों पर की गई उनकी बेलाग टिप्पणियों के कारण उन्हें कई बार संकीर्णतावादियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनकी यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय रही। कई अन्य भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ और 1970 में उनकी मृत्यु के इतने सालों बाद आज भी इसके नए संस्करण निकलते रहते हैं।
इरावती कर्वे ने 11 अगस्त 1970 को पैंसठ वर्ष की अवस्था में सोते हुए अपनी अंतिम साँस ली। उनका जीवन विद्वत्ता, बौद्धिक ईमानदारी, जबर्दस्त मानसिक ऊर्जा और विभिन्न स्तरों पर लोगों के साथ संवाद बना लेने की बेमिसाल क्षमता का नायाब उदाहरण है। भारत में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमिट छाप हमेशा बनी रहेगी।
Iravati Karve was as boisterous as Iravati
अनुवाद: आशुतोष उपाध्याय
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें