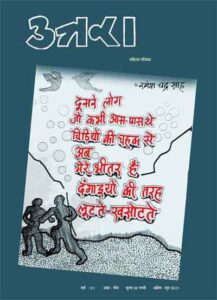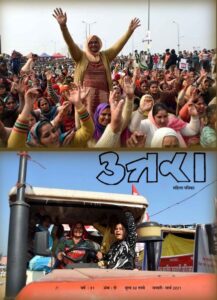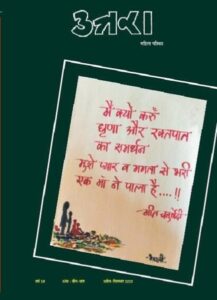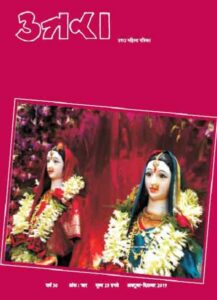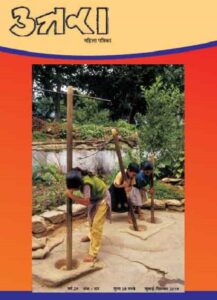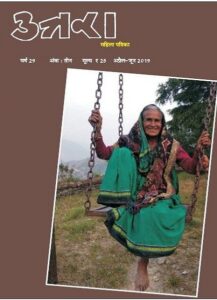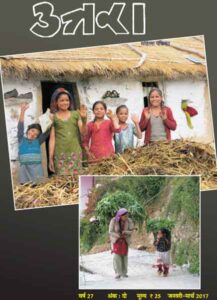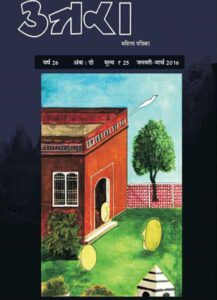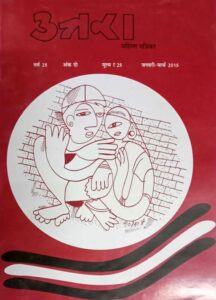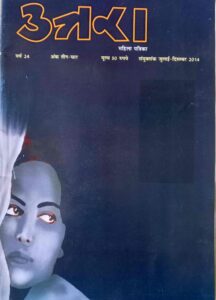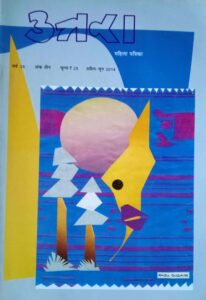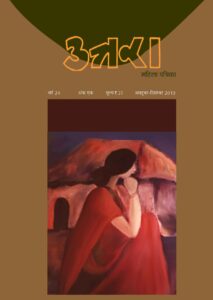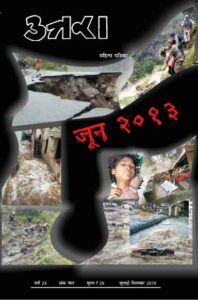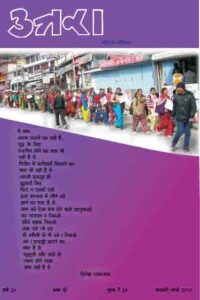आर्थिक सुरक्षा और महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार
गोविन्द केलकर
पिछले अंक से जारी
एशिया में एक बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जो अपनी कमाई अपने हाथ में नहीं रख पातीं। बांग्लादेश और गुजरात में 40 प्रतिशत से ज्यादा और इण्डोनेशिया में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ इस श्रेणी में आती हैं। हालांकि बड़े स्तर पर देखा जाए तो केवल 70 प्रतिशत पत्नियाँ निर्णय लेने में अपने पति से ज्यादा भूमिका निभाती हैं।
अपनी कमाई के इस्तेमाल के तरीकों के लिहाज से चीन में 57 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि रोजमर्रा के घरेलू खर्चों पर वे अपने पतियों से ज्यादा नियंत्रण रखती हैं। हालांकि दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक निर्णय खुद ले सकने वाली महिलाओं की संख्या और भी कम है। इसके अलावा सांस्कृतिक बंधनों के चलते महिलाएँ जायदाद और सम्पत्ति पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पातीं। साथ ही उनकी नौकरी या व्यवसाय से संबंधित आवाजाही की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है।
निवेश के लिए सम्पूर्ण स्वामित्व न सही तो कम से कम इस्तेमाल के सुरक्षित अधिकारों के जरिए अब महिलाओं को सीमित तौर पर इस्तेमाल के हक मुहैया तो हैं लेकिन जब तक ये अधिकार सुरक्षित रूप से उनको हासिल नहीं होते, तब तक वे जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी कमाई नहीं लगाना चाहेंगी। जमीन बेचने के लिए पत्नियों के हस्ताक्षर अनिवार्य होने से स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती, जितनी की जमीन महिला के खुद के नाम पर पंजीकृत होने से होती है। महिलाएँ अक्सर इस्तेमाल के अधिकार की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठाती हैं जैसे कि कोई आदमी अधिकारियों को घूस देकर किसी और महिला को अपनी पत्नी के तौर पर पेश करके जमीन बेच सकता है। जब महिलाएँ खुद अपने नाम पर जमीन खरीदती थीं जैसा कि कुछ महिलाओं ने किया, तब उनकी स्थिति ज्यादा सुरक्षित थी।
जबकि खेती-बाड़ी का ज्यादातर काम महिलाएँ ही संभालती हैं, तब भी उन्हें किसान नहीं माना जाता। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता। इसीलिए कृषि के विस्तार और नई तकनीकों से जुड़ी जानकारी ज्यादातर पुरुषों को ही दी जाती है, जबकि खेती में महिलाओं का योगदान दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम और भारत जैसे देशों में सब्जियों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गयी योजनाओं में ज्यादातर पुरुषों को ही प्रशिक्षित किया जाता रहा है, जबकि दुनियाभर में सब्जियों की खेती मुख्यत: औरतें ही करती हैं। यह जानकारी जब महिलाओं तक पहुँचती है तो अवश्य कुछ अंश छूट जाता है। यदि महिलाओं को मालिक और इस तरह किसानों के रूप में स्वीकारा जाए तो संभव है, उन्हें गृह-प्रबंधकों की तरह ही नहीं बल्कि कृषि प्रबन्धकों की तरह भी देखा जाएगा।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते योगदान के बावजूद जमीन के स्वामित्व अधिकार न होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि जमीन का मालिकाना हक प्राप्त न होने से महिलाओं को संस्थागत ऋण लेने में दिक्कतें पेश आती हैं। उदाहरण के तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों में से बमुश्किल 5 प्रतिशत महिलाएँ हैं। महिलाओं को विस्तार और आगत-आपूर्ति सेवाएँ भी सही वक्त और सही जगह पर मुहैया नहीं हो पातीं। इसलिए जैसे कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने जोर दिया है; महिलाओं के लिए सम्पत्ति की सामान्य परिभाषा है ”ऐसा आर्थिक मानवीय नैसर्गिक अथवा सामाजिक साधनों का भण्डार जिसे हासिल और विकसित किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और आगामी पीढ़ियों के लिए संजोया जा सकता है। यह उपभोग की सामग्री या आमदनी का स्रोत बन सकती है साथ ही अतिरिक्त भंडार भी उत्पन्न कर सकती है।” जमीन एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति के तौर पर अधिकांश उत्पादक ग्रामीण महिलाओं की जरूरत है। जमीन पर अधिकार होने से परिवार और समाज में महिलाओं का रुतबा बढ़ता है और विचार-विमर्श तथा निर्णयों में उनकी स्थिति मजबूत होती है।
सम्पत्ति आधारित नजरिए केवल जीविका के लिए आमदनी का पुनर्वितरण नहीं करते बल्कि ये महिलाओं को आमदनी से संबंधित साधनों के नियंत्रण, इस्तेमाल और परिवर्तन संबंधित नियमों को चुनौती देने और बदलने का दम-खम देते हैं। इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लिंग आधारित सम्पत्ति निर्माण का नजरिया प्रमुख आवश्यकता है।
ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएँ भूमि पर अधिकार हासिल कर लें तो वे स्वतंत्र रूप से कदम लेने, अन्याय और भेदभाव का सामना करने और एक अच्छी जीविका चलाने लायक स्वतंत्रता हासिल कर लेती हैं। सम्पत्ति के प्रभाव से लोगों का नजरिया और व्यवहार बदल जाता है। अगर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई नीति बनाई जा रही हो तो उसमें महिलाओं के हितों को शामिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। नीतियाँ इस मकसद से बनाई जानी चाहिए कि समाज का जो वर्ग पीछे छूट गया है उसे खासकर औरतों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। साथ ही उन्हें अपने नाम पर स्वतंत्र रूप से उचित साधनों का स्वामित्व प्राप्त हो, जिससे अपने परिवार द्वारा हासिल सामाजिक सुरक्षा में वे भी हिस्सेदार बन सकें। सम्पत्ति के स्वामित्व से कुशलता में बढ़ोत्तरी होती है और अन्य कामों के लिए समय और मेहनत कर पाने की संभावनाएँ बढ़ती हैं जिससे समुदाय में रुतबा और प्रभाव बढ़ता है।
बग्लादेश की मत्स्य पालन परियोजना इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस परियोजना में केवल महिलाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें अपने पुरुषों के तालाबों में व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए ऋण सुविधाएँ दी गईं। इस ज्ञान और मदद के जरिए महिलाओं ने उत्पादकता में पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल कर मछली पालन को रोजी-रोटी के स्तर से व्यावसायिक स्तर तक पहुँचा दिया। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने छोटे कर्जों की मदद से यदाकदा जोती जाने वाली जमीनों को लीज पे लेकर उन्हें ज्यादा उत्पादकता वाली नियमित कृषि भूमि में बदल दिया।
Economic security and property rights of women
महिलाओं की सामान्य आर्थिक स्थिति सुधरने से और साथ ही जमीन, पशुधन और ऊर्जा सरीखे साधनों पर उनका नियंत्रण मजबूत होने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा घट सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने से अपने आप हिंसा नहीं रुकती लेकिन इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्थिति मजबूत होती है और वे हिंसा का प्रतिरोध करने में ज्यादा सक्षम हो पाती हैं।
एशियाई देशों में सूक्ष्म वित्त महिलाओं के लिए जमीन हासिल करने के लिए पूँजी का जरिया बन गया है। हालांकि बांग्लादेश की सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ महिलाओं को कर्ज लेकर जमीन लेने की सलाह नहीं देतीं, क्योंकि जमीन से न तो जल्द आमदनी होनी शुरू होती है और न ही इससे नियमित रूप से आमदनी होती है। लेकिन इसके बावजूद अकसर महिलाएँ अपनी पूँजी के साथ अपने पतियों की वित्तीय सहायता जोड़कर कर्ज लेकर जमीनें लीज पर लेती हैं। जमीन की खरीददारी फिर भी कम देखने को मिलती है, लेकिन लीज पर जमीनें लेने का सिलसिला ऋण समूहों की महिला सदस्यों में काफी प्रचलित है। ग्रामीण बांग्लादेश पर एक रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग ऋण समूहों की कुल 261 महिलाओं में से 117 ने जमीन खरीदी या लीज पर ली। इनमें से 87 मामलों में जमीन महिलाओं के नाम थी। दस मामलों में दो महिला समूहों ने मिलकर सब्जियाँ उगाने के लिए जमीन लीज पर ली थी। चार मामलों में पति-पत्नी ने संयुक्त रूप से जमीन ली थी जबकि 26 मामलों में केवल पति के ही नाम पर जमीन ली गई थी। भारत में दक्कन विकास सोसाइटी ने जानबूझकर जमा पूँजी और ऋण के जरिए महिला समूहों को लीज पर जमीनें दिलाई हैं। ज्यादा गरीब महिलाओं के लिए पैसे की जगह मजदूरी करके भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। समूहों के तौर पर जमीनें लीज पर लेने से बाजार में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। इससे वो ज्यादा जमीन लीज पर ले पाती हैं। महिला समूहों ने 26 गाँवों में पास के जंगलों का निर्माण करके 1,000 एकड़ सार्वजनिक जमीन को विकसित किया। अब जमीनों के दस्तावेज उन्हीं के नाम पर हैं।
आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथारिटी और सेड्यूलकास्ट डेवलपमेंट काउंसिल जैसी सरकारी संस्थाओं ने जमीन लीज पर देने के इच्छुक लोगों से जमीनें लेकर जमीन से वंचित लोगों को मुफ्त जमीनें दीं। ये सभी जमीनें महिलाओं के नाम हस्तान्तरित की गई हैं। चेंचू समुदाय में भी जमीनें महिलाओं के नाम हस्तांतरित की गयी हैं। चेंचू पुरुषों का भी यही मानना है कि महिलाएँ आम तौर पर शराब या जुए के कारण जमीन नहीं गँवाती हैं। महिलाएँ सरकारी भूमि सुधारों की प्रतीक्षा किए बिना पूँजी और बाजार प्रणाली के जरिए जमीनें हासिल कर रही हैं।
लिंग के आधार पर जिम्मेदारियों में भिन्नता के कारण महिलाएँ और पुरुष जमीन और वनों के उपयोग को लेकर अलग-अलग नजरिया रखते हैं। पैसा कमाना पुरुषों की मुख्य जिम्मेदारी होने के कारण वे इमारती-लकड़ी (Timber) के वृक्षों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। दूसरी ओर महिलाओं की जिम्मेदारियों में भोजन की व्यवस्था शामिल होने से वे बहु-उपयोगी पेड़ों के पक्ष में रहती हैं, खासकर जिनसे ईंधन और चारे की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।
एशिया के ऊपरी इलाकों में कृषि तौर-तरीकों के तीव्रीकरण की समीक्षा करने पर पता चलता है कि वनों से ईंधन लाने की क्रिया का सबसे आखिर में तीव्रीकरण हुआ। इसका यह कारण था कि महिलाओं द्वारा ईंधन जुटाने में किए गए श्रम की विकल्प-लागत कम होने के कारण उनके श्रम का और उसके द्वारा जुटाए गए ईंधन का अपव्यय होता रहा था।
कई कारणों से महिलाओं को खेती के लिए कम सक्षम माना जाता रहा है। लेकिन हाल में चीन में महिला प्रधान परिवारों द्वारा धान, गेहूँ और मकई की फसलों की खेती पर अध्ययन से यह कथन असत्य सिद्ध होता है। छ: प्रान्तों के 600 गाँवों में 5,000 से अधिक आंकड़ों की सहायता से लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महिलाओं द्वारा खेती किए जाने पर कम से कम उतनी आमदनी तो होती है, जितनी पुरुषों के खेती करने पर होती है।
इसी तरह 2003-04 में कृषि विज्ञान केन्द्र ने आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित डेरी इकाइयों पर अध्ययन किया और यह पाया कि प्रति-इकाई दुग्ध उत्पादन 380 से बढ़कर 610 लीटर हो गया है और मुनाफा रुपया 3,20,000 से बढ़कर 5,80,000 प्रति इकाई प्रति वर्ष हो गया है।
Economic security and property rights of women
हाल ही में फरीदपुर की मत्स्य पालन विकास परियोजना (बांग्लादेशी सरकार और आईएफडी की साझेदारी में) के अंतर्गत तालाब-मालिकों की पत्नियों को प्रशिक्षण दिया गया और पूँजी मुहैया कराई गई। इससे महिलाएँ घर की आमदनी और उस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने में सफल हुईं। हालांकि तालाब तो उनके पतियों के ही नाम थे लेकिन मछली पालन उद्योग उनका अपना था। एक महिला के शब्दों में ”तालाब तो मेरे पति का है, पर इसमें मछलियाँ मेरी हैं।” मछली पालन क्रिया से उत्पन्न आमदनी से महिलाओं ने पशुधन, दुकानें इत्यादि खरीदे हैं और जमीनें लीज पर ली हैं। उनके अंदर अधिकारियों और अन्य बाहरी व्यक्तियों से बात करने की हिम्मत बढ़ी है। उनके आत्मसम्मान और परिवार और गाँव में उनकी इज्जत में भी इजाफा हुआ है।
दोनों उदाहरण सम्पत्ति के प्रबंधन के तरीकों में बदलाव के हैं। पहले में सरकारी सम्पत्ति महिलाओं को सौंपी गई, दूसरे में महिलाओं ने पूँजी और ज्ञान की मदद से अपने पतियों के हाथ से तालाबों का वास्तविक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।
महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्पत्ति पर स्वतंत्र अधिकार दिलाना और प्रबंधन का हुनर सिखाया जाना भी जरूरी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में सूचना और संचार के माध्यम का उपयोग करके ग्रामीण समाज को लिंग-संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे महिलाओं का किसान, निर्माता और आर्थिक योगदाता के तौर पर देखा जाना संभव हो सके।
कमोबेश सभी एशियाई देशों में महिला-अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून मौजूद हैं लेकिन उनके लागू होने के स्तर अलग-अलग हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की नीतियाँ उत्पादक सम्पत्ति की प्रणाली के लैंगिक असमानता के चलते महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता को लगातार नजरअंदाज करती रही हैं। महिलाओं के लिए अपने स्वतंत्र मत का प्रयोग कर पाने के लिए हिंसा और दबाव मुक्त होना जरूरी है। एक तर्क यह भी है कि महिलाएँ इस भय से तभी मुक्त हो पाएंगी जब उत्पादक पूँजी पर उनका स्वतंत्र अधिकार और नियंत्रण होगा और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगी।
भारत में उत्पादक पूँजी के लैंगिक वितरण से संबंधित नीतिगत प्रश्नों को समझने के लिए कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना जरूरी है। नीतियों में विचार करने योग्य तीन मुख्य प्रश्न हैं- 1. कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों में बदलाव 2. एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सम्पत्ति वितरण में लैंगिक असमानता का उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रभाव 3. जमीन और अन्य उत्पादक साधनों पर महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी में नीतियों में उपयुक्त बदलावों को प्राथमिकता।
भारत के योजना-संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के अनुकूल योजनाओं में फेरबदल करने में विशेष चुनौती नहीं है लेकिन मौजूदा प्रशासनिक तंत्र को महिलाओं के हितों के लिए ज्यादा असरदार ढंग से काम करने के लिए ढालना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निर्मित नीतिगत ढाँचे को लागू करने के लक्ष्यों पर जोर नहीं दिया गया है। लैंगिक समानता की सामाजिक समीक्षाओं और लैंगिक संवेदना जगाने के लिए बनाए गये कार्यक्रमों को लागू करने में होने वाली खामियों को उजागर करना चाहिए। चिरस्थाई विकास गति के लिए और नीतियों की सुस्त चाल (प्रवृत्ति) को दूर करने के लिए ऐसी रणनीति की जरूरत है जिससे नीतियों को सही ढंग से लागू करके और सम्पत्ति का उचित पुर्निवतरण करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके (नारायण मूर्ति 2007)।
किसी भी समुदाय के आंतरिक सामाजिक सम्बन्र्ध लिंग-निरपेक्ष नहीं होते। इसी तरह जमीन के पुर्निवतरण के नतीजे भी लिंग-सापेक्ष होते हैं। यह माना गया है कि विकास नीतियों और अध्ययनों में परिवार को इकाई के रूप में देखने से सामाजिक अनुक्रम और लिंग भेद उजागर नहीं होते।
ऐसे में सुरक्षा और सशक्तीकरण जैसे जटिल मसलों का अतिसरलीकरण करके उन्हें मात्र स्थानीय लोगों के सामने समस्याओं के तौर पर रखा जा रहा है जबकि समुदाय या परिवार के आंतरिक सत्ता-समीकरणों या सम्पत्ति-नियंत्रण के प्रश्नों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है।
महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और नीतियों को लागू कराने के लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत/ संस्थात्मक प्रबंध होने जरूरी हैं। साथ ही सरकारी नीतियों के निर्माण स्तर पर जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि लैंगिक समानता लाने वाले कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मनरेगा के सामाजिक अवलोकनों की तर्ज पर उनमें जवाबदेही तय करने के लिए प्रावधान रखे जांए। जाहिर है ऐसा होने से देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। यदि महिलाओं को भी पुरुषों की तर्ज पर उत्पादक सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त होंगे तो उससे आर्थिक गतिविधियाँ बढेंगी और महिलाओं के पुरुषों पर निर्भर होने का सामाजिक दृष्टिकोण बदलेगा। इससे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में महिलाएँ ज्यादा संख्या में शामिल होने लगेंगी, उनकी विविध क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ावा भी मिलेगा।
साभार: नामाबर अक्टूबर, 2011
Economic security and property rights of women
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें